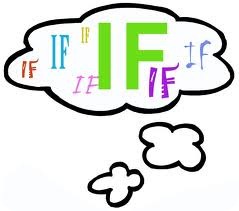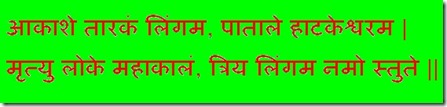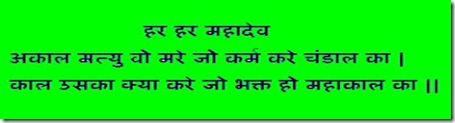करीबन ढ़ाई वर्ष पहल मुँबई से बैंगलोर आये थे तो हम सभी को भाषा की समस्या का सामना करना पड़ा, हालांकि यहाँ अधिकतर लोग हिन्दी समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो हिन्दी समझते हुए जानते हुए भी हिन्दी में संवाद स्थापित नहीं करते हैं, वे लोग हमेशा कन्नड़ का ही उपयोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिन्दीभाषी जरूर हैं परंतु दिन रात इंपोर्टेड अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, इसी में संवाद करते हैं।
जब मुँबई गया था तब लगता था कि सारे लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं, परंतु बैंगलोर में आकर अपना भ्रम टूट गया । कम से कम मुँबई में हिन्दी भाषा अच्छे से सुनने को मिल जाती थी, यहाँ भी मिलती है परंतु बहुत ही कम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हिन्दी भाषा का उपयोग मजबूरी में करते हैं क्योंकि आज बैंगलोर में लगभग ८०% लोग जो कि सॉफ़्टवेयर कंपनियों में हैं वे हिन्दी भाषी हैं, अगर स्थानीय लोग हिन्दी नहीं समझेंगे तो उनकी रोजी रोटी की समस्या हो जायेगी।
अधिकतर दुकानदार हिन्दी अच्छी समझ लेते हैं और बोल भी लेते हैं, जब वे अपनी टूटी फ़ूटी हिन्दी में बोलते हैं तो अच्छा लगता है, रोष नहीं होता कि हिन्दी गलत बोल रहे हैं, खुशी होती है कि सीख रहे हैं, और सीखना हमेशा गलत से ही प्रारंभ होता है। हमने भी कन्नड़ के थोड़े बहुत संवाद सीख लिये हैं, जिससे थोड़ा आराम हो गया है। हम सुबह सुबह जब दूध लेने जाते हैं तो अगर बड़ा नोट देते हैं और कहते हैं “भैया, छुट्टा देना” बाद में अहसास होता है कि पता नहीं यह समझेगा भी कि नहीं, परंतु समझ लेता है तो अब आदत ही बन गई है।
जब बैंगलोर आये थे, तो हमारे बेटेलाल बहुत ही हतप्रभ थे और कहते थे कि “डैडी ये कैसे इतनी प्रवाह में कन्नड़ बोल लेते हैं”, हमने कहा “जैसे आप हिन्दी प्रवाह में बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, वैसे ही इनकी कन्नड़ मातॄभाषा है, ये बचपन से कन्नड़ के बीच ही पले हैं”, बेटेलाल की समझ में आ गया। पर बेटेलाल ने कभी कन्नड़ सीखने की कोशिश नहीं की। पहले एक महीना चुपचाप निकाला, हिन्दी में बात करने की कोशिश की परंतु नाकाम, छोटे बच्चे अधिकतर जो स्थानीय थे, वे या तो कन्नड़ समझते थे या फ़िर अंग्रेजी समझते थे। बेटेलाल को अंग्रेजी से इतना प्रेम था नहीं, क्योंकि मुँबई में हिन्दी से अच्छे से काम चल जाता था, और यहाँ बैंगलोर में आकर फ़ँस गये, कई बार बोले “डैडी चलो वापिस मुँबई चलते हैं, यहाँ बैंगलोर में अच्छा नहीं लग रहा ।” हमने कहा देखो बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। बस तो अगले दिन से ही फ़र्राटेदार अंग्रेजी शुरू हो गई।
अब बेटेलाल का काम तो निकल पड़ा, अब समस्या आई तब जब घर के आसपास कुछ दोस्त बनें, वो भी स्थानीय पहले वे हिन्दी में बात करने से इंकार करते थे, परंतु उनके अभिभावकों ने समझाया कि इनकी हिन्दी अच्छी है, हिन्दी में बात करो और हिन्दी सीखो। पर हमारे बेटेलाल अपने दोस्तों से हिन्दी में संवाद करने को तैयार ही नहीं होते हैं, वे उनसे अंग्रेजी में ही बात करते हैं। खैर इसका हल हमने निकाला कि हम हिन्दी में बात करेंगे।
कभी कभार अगर गलती से अंग्रेजी में घर पर बेटेलाल को कुछ बोल भी दिया तो सीधे बोलते हैं “डैडी, मैं बाहर तो अंग्रेजी ही बोलता हूँ, कम से कम घर में तो हिन्दी में बात करो, नहीं तो मैं हिन्दी भूल जाऊँगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा ?”
खैर अब बैंगलोर में मेरे लिये वह नयापन नहीं रह गया, अब यहाँ के अभ्यस्त हो गये हैं, जहाँ भी काम होते हैं अब पता चल गया है कि हिन्दी अधिकतर उपयोग होती है, और अगर हिन्दी ना समझ में आये तो अंग्रेजी से तो काम हो ही जायेगा ।